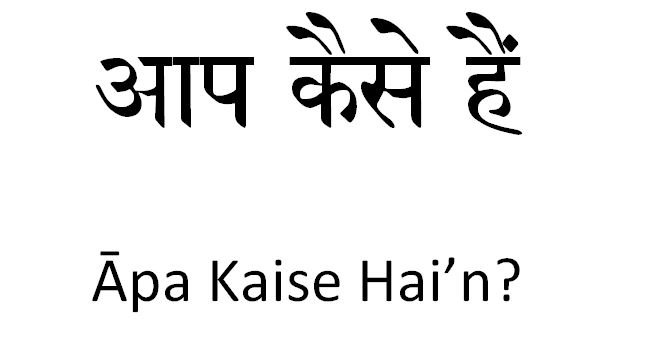संधि (Union of Two Sounds)
सन्धि – दो वर्णों के मेल को भाषा में सन्धि कहा जाता है। दो शब्दों में सन्धि के समय पहले शब्द का अन्तिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिल जाते हैं। जैसे -
परम + आत्मा = परमात्मा
यहाँ पर परम शब्द का अन्तिम वर्ण अ है और आत्मा शब्द का प्रथम वर्ण आ है। दोनों के मिलने से आ बना -
अ + आ = आ
सन्धि के निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं -
- स्वर सन्धि
- व्यञ्जन सन्धि
- विसर्ग सन्धि
स्वर सन्धि – जब मिलनेवाले दो शब्दों में से पहले शब्द का अन्त का और दूसरे शब्द का आरम्भ के स्वर का मेल हो तो इस प्रकार होनेवाली सन्धि को स्वर सन्धि कहते हैं। जैसे -
| विद्या + आलय = विद्यालय | आ + आ = आ |
| विद्या + अर्थी = विद्यार्थी | आ + अ = आ |
| रवि + इन्द्र = रवीन्द्र | इ + इ = ई |
| यदि + अपि = यद्अपि | इ + अ = य |
| इति + आदि = इत्यादि | इ + आ = या |
| सु + आगत = स्वागत | उ + आ = वा |
| पर + उपकार = परोपकार | अ + उ = ओ |
| महा + ऋषि = महर्षि | आ + ऋ = अर् |
| सदा + एव = सदैव | आ + ए = ऐ |
| ने + अन = नयन | ए + अ = अय् |
| पो + अन = पवन | ओ + अ = अव् |
| नै + अक = नायक | ऐ + अ = आय् |
व्यञ्जन सन्धि – जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अन्त में व्यञ्जन का और दूसरे शब्द का आरम्भ के स्वर या व्यजन का मेल हो तो इस प्रकार होनेवाली सन्धि को व्यञ्जन सन्धि कहते हैं। जैसे -
| दिक् + अंबर = दिगंबर |
| सत् + आचार = सदाचार |
| सत् + मार्ग = सन्मार्ग |
| जगत् + ईश्वर = जगदीश्वर |
| सत् + जन = सज्जन |
| दिक् + गज = दिग्गज |
| उत् + ज्वल = उज्जवल |
| जगत् + गुरू = जगद्गुरू |
| उत् + लास = उल्लास |
| उत् + घाटन = उद्घाटन |
| उद् + साह = उत्साह |
| शरत् + चन्द्र = शरच्चन्द्र |
| सद् + कार = सत्कार |
| जगत् + नाथ = जगन्नाथ |
| सत् + भावना = सद्भावना |
विसर्ग सन्धि – जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अन्त में विसर्ग (:) का और दूसरे शब्द का आरम्भ में स्वर या व्यञ्जन का मेल हो तो इस प्रकार होनेवाली सन्धि को विसर्ग (:) सन्धि कहते हैं। जैसे –
| नि: + संदेह = निस्संदेह |
| मन: + योग = मनोयोग |
| तप: + वन = तपोवन |
| दु: + चरित्र = दुश्चरित्र |
| दुः + गुण = दुर्गुण |
| नि: + तेज = निस्तेज |
| मन: + हर = मनोहर |
| नि: + कण्टक = निष्कण्टक |
| पुन: + आगमन = पुनरागमन |
| नि: + फल = निष्फल |
| अन्त: + दशा = अन्तर्दशा |
| रज: + गुण = रजोगुण |
| नि: + आशा = निराशा |
याद रखने योग बात – सन्धि, तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ अन्य शब्दों में भी होती है। जैसे -
| अब + ही = अभी |
| जो + ने = जिसने |
| जब + ही = जभी |
| वह + ने = उसने |
| तब + ही = तभी |
| वे + ने = उन्होंने |
| कब + ही = कभी |
| कौन + ने = किसने |
| यह + ही = यही |
| हर + एक = हरेक |
| यहाँ + ही = यहीं |
| वहाँ + ही = वहीं |
| कहाँ + ही = कहीं |
| यह + ने = इसने |
| इन + ने = इन्होंने |
| कान + कटा = कनकटा |